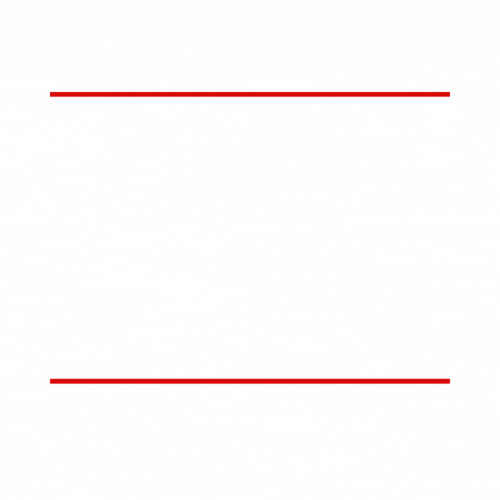यह दिन केवल तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण नहीं_मिथलेश


चंद्रशेखर मिथलेश, शासकीय आशी बाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महासमुंद
*डिजिटल भारत की संचार गाथा*
“संचार वह पुल है, जो विचारों को जोड़ता है और समाज को आगे बढ़ाता है।” हर साल 17 मई को पूरी दुनिया ‘विश्व दूरसंचार दिवस’ के रूप में मनाती है। यह दिन केवल तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी क्रांति का उत्सव है जिसने समय, स्थान और सीमाओं को लांघते हुए इंसानों को जोड़े रखने की राह दिखाई है। इसकी शुरुआत 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union – ITU) की स्थापना से हुई थी। 1969 में पहली बार यह दिवस मनाया गया और 2005 में इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ‘विश्व सूचना समाज दिवस’ का रूप दिया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा लाए गए सामाजिक परिवर्तन के प्रति वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करना है।
आज हम ऐसे युग में हैं जहाँ तकनीक ने हमें अभूतपूर्व ऊँचाइयों तक पहुँचाया है, परंतु एक सच्चाई यह भी है कि लगभग 2.6 बिलियन लोग अभी भी इंटरनेट से वंचित हैं। इनमें से अधिकांश महिलाएँ और लड़कियाँ हैं, जो डिजिटल दुनिया में पूर्ण भागीदारी से वंचित हैं। डिजिटल उपकरणों की पहुँच, affordability और कौशल के अभाव ने एक नया सामाजिक अंतराल खड़ा कर दिया है। इस अंतर को पाटे बिना हम नवाचार, आर्थिक विकास और समावेशी समाज की कल्पना नहीं कर सकते।
जगदीश चंद्र बोस पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया एवं उन्हें रेडियो विज्ञान का पिता माना जाता है। 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर संचार क्रांति का आरंभ किया। उनका पहला संदेश – “Mr. Watson, come here – I want to see you” – तकनीक और भावना का अनोखा संगम था। इसके बाद वैज्ञानिकों की श्रृंखला ने वायरलेस संचार को जन्म दिया। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने विद्युत-चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो आज के रेडियो, टीवी, मोबाइल और Wi-Fi जैसी तकनीकों की आत्मा है। हेनरिक हर्ट्ज़ ने इन तरंगों को प्रयोगशाला में सिद्ध कर तकनीक को गति दी।
भारत में सैम पित्रोदा ने C-DOT की स्थापना कर ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति लाई। डॉ. विक्रम साराभाई और डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भारत को उपग्रह संचार प्रणाली से जोड़ा। प्रो. भास्कर राममूर्ति और उनकी IIT मद्रास की टीम ने स्वदेशी 5G तकनीक पर कार्य किया। वहीं डॉ. एम.जी.के. मेनन ने नीति और अनुसंधान को दिशा दी। इन वैज्ञानिकों ने भारत को तकनीकी आत्मनिर्भरता और डिजिटल समावेशन की राह पर अग्रसर किया।
जहाँ विकसित देश अभी 5G में उलझे हैं, भारत 6G की दिशा में तेजी से अग्रसर है। यह तकनीक 5G से 100 गुना तेज होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रक्षा जैसे क्षेत्रों में एक नए युग की शुरुआत करेगी। भारत अब केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्वकर्ता बनने की ओर बढ़ रहा है।
डिजिटल समाज ने शिक्षा, टेलीमेडिसिन, स्टार्टअप, ई-गवर्नेंस और नागरिक सहभागिता को नया आयाम दिया है। परंतु इसके साथ साइबर अपराध, फेक न्यूज़ और युवाओं में तकनीकी लत जैसी गंभीर चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। हमें यह स्वीकारना होगा कि तकनीक एक अमूल्य वरदान है, परंतु विवेकहीन प्रयोग इसे अभिशाप में बदल सकता है।
दूरसंचार की यह यात्रा किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह विज्ञान की गहराइयों से निकलकर आज हमारे हाथों में स्मार्टफोन बनकर उपस्थित है। आईटीयू, C-DOT, TRAI जैसे संगठनों की दूरदृष्टि, वैज्ञानिकों का सतत अनुसंधान और जनसामान्य की तकनीक तक पहुँच — मिलकर एक ऐसा भारत गढ़ते हैं जो संवादशील, सशक्त और आत्मनिर्भर है।
17 मई केवल एक तिथि नहीं, बल्कि यह स्मरण है उस यात्रा का, जहाँ विज्ञान, तकनीक और मानवता मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करते हैं जो संवाद को केवल शब्द नहीं, बल्कि संस्कार बनाते है।